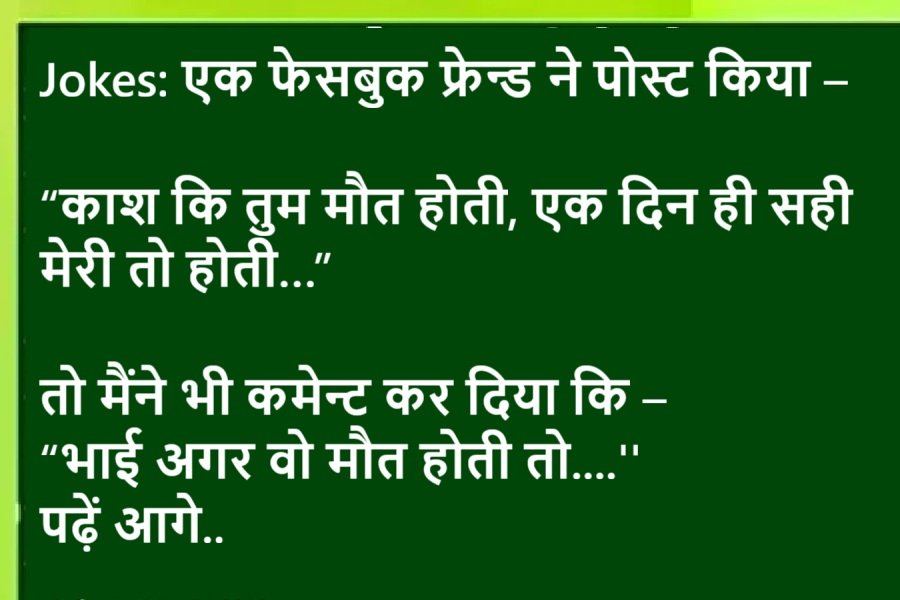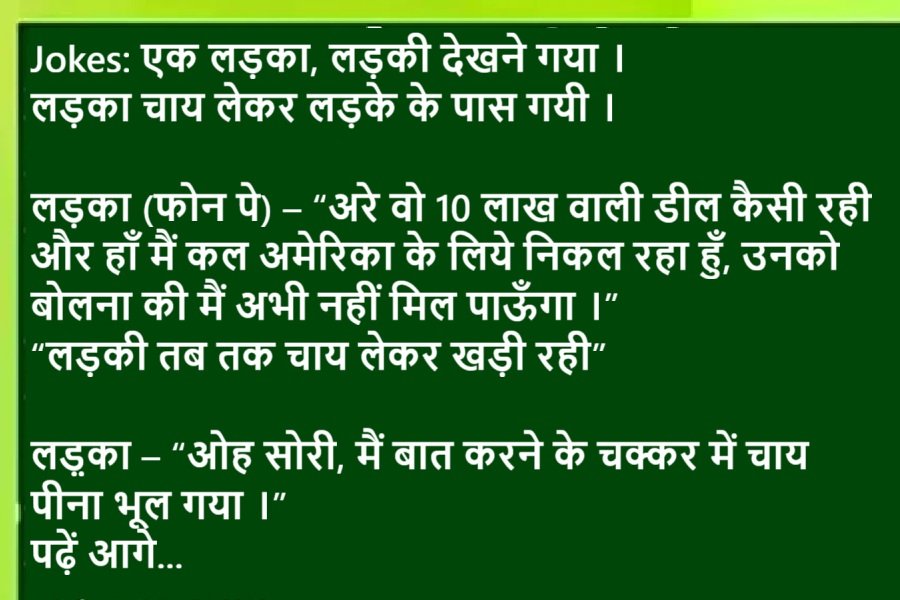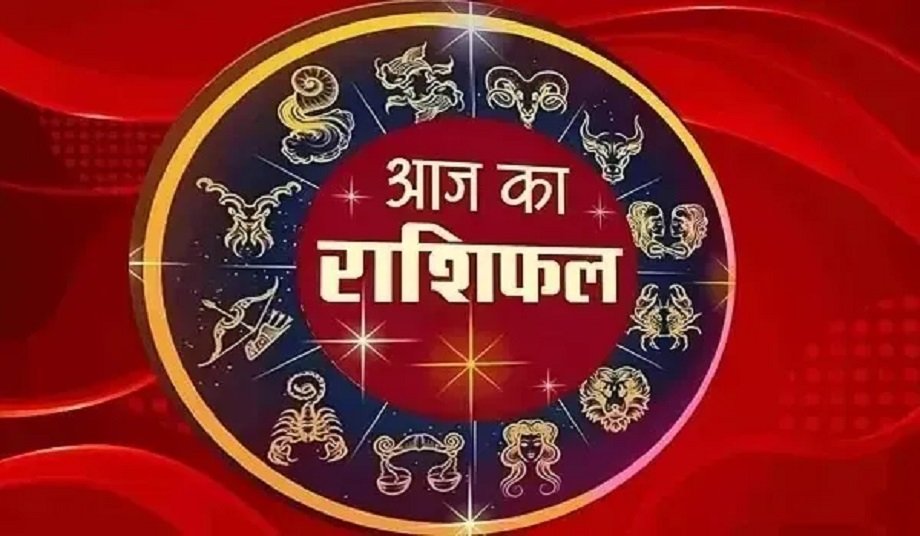Geeta: अत्यधिक चिंतन से होती है मानसिक पीड़ा, मन नहीं रह पात शांत, भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है इसका उपाय
- byvarsha
- 04 Aug, 2025

PC: saamtv
आज की तनावपूर्ण दुनिया में, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और नकारात्मक विचार मानसिक परेशानी का एक बड़ा कारण बन गए हैं। मन अनगिनत विचारों से भरा रहता है, एक छोटी सी चिंता पहाड़ जैसी लगती है और हमारी नींद, शांति और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। लेकिन यह समस्या सिर्फ़ आज की नहीं है। हज़ारों साल पहले, कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में अर्जुन भी ऐसे ही विचारों में उलझे हुए थे। उस समय श्रीकृष्ण ने उन्हें तलवार नहीं, बल्कि उस समय दिया गया ज्ञान दिया था।
भगवत गीता सिर्फ़ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह आपको मानसिक रूप से मज़बूत बनाने का एक मार्गदर्शक है। इसका ज्ञान आज भी उतना ही उपयोगी है जितना कि आज। नीचे दिए गए अध्याय निश्चित रूप से भगवत गीता की मदद से आपके मन को शांत करने में आपकी मदद कर सकते हैं।
मन का अस्थिर होना
गीता के छठे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन स्वीकार करते हैं, "मन अस्थिर, चंचल, हठी है। इसे रोकना हवा को पकड़ने के समान है।" हमारा मन भी ऐसा ही है। निरंतर चिंतन, चिंता और चिन्ता में लगे रहना। श्रीकृष्ण अर्जुन की इस परेशानी को कम नहीं आँकते, बल्कि कहते हैं कि 'अध्ययन' और 'वैराग्य' की सहायता से मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है।
दर्शन पाठ:
यदि हम अत्यधिक सोच रहे हैं, तो स्वयं को दोष न दें। मूलतः, यह मन का स्वभाव है। लेकिन यह स्थायी नहीं है। प्रयास की निरंतर आदत मन को नियंत्रित कर सकती है।
वैराग्य उदासीनता नहीं है
गीता का एक महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझा जाने वाला संदेश 'वैराग्य' है। इस शब्द को सुनकर कई लोग सोचते हैं कि हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए। लेकिन श्रीकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कर्म करते रहो, लेकिन फल की इच्छा मत करो।
अत्यधिक सोचना अक्सर इसी बात के कारण होता है, "क्या होगा अगर?", "लोग क्या कहेंगे?", "अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा?" ये सभी विचार हमें भविष्य में फँसाए रखते हैं।
दर्शन पाठ:
कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। भविष्य में मत जियो, वर्तमान में जियो। यदि आप परिणामों की अपेक्षा करते हैं, तो चिंता और भ्रम दोनों कम हो जाएँगे।
वर्तमान में एकाग्रता ही सच्चा कर्म योग है।
श्रीकृष्ण बार-बार 'कर्म योग' पर ज़ोर देते हैं, जिसका अर्थ है निःस्वार्थ कर्म। इसमें मुख्य बात है अपना पूरा ध्यान वर्तमान कार्य पर केंद्रित करना। अति-विचार ज़्यादातर खाली समय में या एक साथ कई काम करते समय होता है। लेकिन जब हम कोई काम एकाग्रता से करते हैं, जैसे खाना बनाना, लिखना, कोई मीटिंग, तो मन को भटकने की कोई गुंजाइश नहीं रहती।
दर्शन का पाठ:
अपने आप को वर्तमान क्षण में बाँध लें। अपने मन, शरीर और आत्मा को उस कार्य पर केंद्रित करें जो आप कर रहे हैं। यह ध्यान का एक रूप है और अति-विचार का एक बेहतरीन उपाय है।
मन की 'पसंद-नापसंद' के खेल से परे देखना ज़रूरी है
गीता के दूसरे अध्याय में, श्री कृष्ण कहते हैं, "सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय, सबको समान रूप से समझो।" हम अपने मन में हर चीज़ को "यह अच्छा है", "यह बुरा है", "मैं हीन हूँ", "वे कितनी दूर चले गए हैं" जैसे लेबल लगाते हैं। ये विचार हमारी भावनाओं में उतार-चढ़ाव पैदा करते हैं और इस तरह विचारों को और उलझा देते हैं।
दर्शनशास्त्र का पाठ:
हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। बल्कि, बस विचारों का अवलोकन करें। क्या यह विचार सचमुच सच है? खुद से पूछें। विचारों को अस्वीकार न करें, लेकिन उनका शिकार भी न बनें।